वैश्विक दक्षिण के लिए विकास के एक नए सिद्धांत की खोज
नवउदारवाद के मंसूबों को तभी नाकाम किया जा सकता है जब तमाम ग़रीब देश अपने लिए विकास का एक नया सिद्धांत तैयार करें।
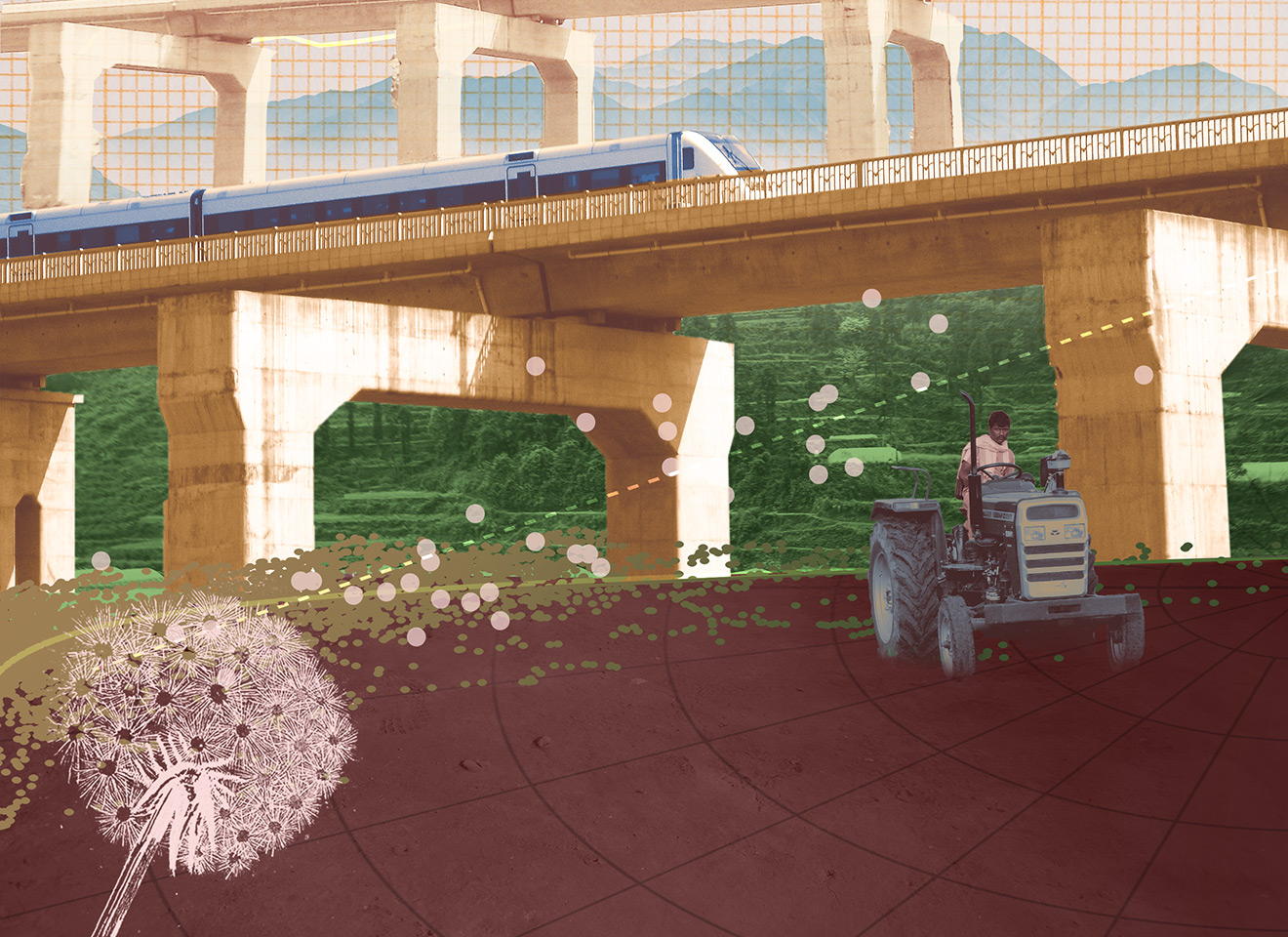
![]()
दुनिया भर में प्रगतिशील सरकारें ज़रूर सत्ता में आई हैं, लेकिन अब तक उनके पास अपने समाजों को नवउदारवाद के चरमराते ढाँचे से निकालकर उनका नवनिर्माण करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। होंडुरास, सेनेगल और श्रीलंका जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क़र्ज़ और ख़र्चों में कटौती पर आधारित प्रणाली की अपनी आलोचना में बहुत स्पष्ट हैं, मगर इनके पास इससे आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। नवउदारवाद से अलग एक नीति बनाने में असफल होने की वजह इनमें से कई सरकारें वापस नवउदारवादी दलदल में फँस जाती हैं।
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी एक वैकल्पिक व्यवस्था पेश करने में असफल रहे हैं। लेकिन 2000 में एक ऐसी कोशिश हुई थी, जब यूएन ने ग़रीबी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ज़ोर देने के लिए आठ मिलेनियम डेवेलप्मेंट गोल्स (एमडीजी) निर्धारित करते हुए विकास के परिणाम आधारित लक्ष्यों को केंद्र में लाने की प्रक्रिया शुरू की।1 एमडीजी के बाद 2015 में सत्रह सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवेलप्मेंट गोल्स, एसडीजी) आए जिन्हें 2030 तक पूरा किया जाना है। लेकिन एमडीजी की ही तरह एसडीजी भी बिना किसी सिद्धांत या कार्यक्रम के बहुत सारे लक्ष्यों की एक कोरी रूपरेखा ही प्रदान करते हैं।
इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि यूएन की 2023 की रिपोर्ट में लिखा गया कि कई एसडीजी ‘अपने लक्ष्य से काफ़ी हद तक या बहुत ज़्यादा भटक गए’ हैं। रिपोर्ट में इस असफलता की वजह तीसरी आर्थिक महामंदी (2006-2007), कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और फ़िलिस्तीनियों के जनसंहार को बताया गया है। 140 लक्ष्यों में से महज़ 12% ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जबकि 50% अपने लक्ष्य से काफ़ी हद तक या बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं और 30% में काम उसी जगह रुका हुआ है या पिछड़ गया है।2
वे लोग जो एसडीजी की कार्यप्रणाली के पक्ष में बोलते हैं उनका कहना है कि स्थिति बेहतर करने के लिए फंड में इज़ाफ़ा करना होगा। लेकिन यह सोच इस सच्चाई को नज़रंदाज़ करती है कि पश्चिम के वर्चस्व वाली वित्तीय व्यवस्था की तरफ़ से फंड मिल ही नहीं रहा। मौजूदा स्थिति यह है कि 2030 तक एसडीजी के लक्ष्य पूरा करने के लिए ज़रूरी सालाना धन में हर वर्ष 4 लाख करोड़ डॉलर की कमी रह रही है।3 1970 में वैश्विक उत्तर के देशों ने वादा किया था कि वे अपनी सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का 0.7% ऑफ़िशियल डेवेलप्मेंट असिस्टेंस (यानी विदेशों की सहायता) के लिए खर्च करेंगे। इस लिहाज़ से यह एसडीजी कार्यक्रमों के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन यह खर्च नहीं किया गया: 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने अपनी जीएनआई का सिर्फ़ 0.24% विकास सहायता के लिए खर्च किया, फ़्रांस ने महज़ 0.5% और यूनाइटेड किंगडम ने 0.58% (दूसरी तरफ़ 2014 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने सदस्यों ने वादा किया कि वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% युद्धों पर खर्च करेंगे)।4 और तो और, वैश्विक दक्षिण के जो देश अपनी विकास योजनाओं को एसडीजी के मुताबिक़ तैयार करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहायता, क़र्ज़, विकास कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क़र्ज़ मिलने में आसानी होनी चाहिए। इसके बावजूद क़र्ज़ मिलना अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि वे देश ‘मुक्त बाज़ार सुधारों’ को कितना अपनाते हैं (जिसमें खर्चों में कटौती की नीतियाँ, अविनियमन और सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल है)। इस तरह ग़रीब देशों को एसडीजी लक्ष्य पूरा करने और विकास कार्यों के लिए निवेश लाने के लिए ‘प्रोत्साहित’ (असल में, मजबूर) किया जाता है कि वे और क़र्ज़ लें या अपनी अर्थव्यवस्थाएं पश्चिमी निवेशकों के लिए खोल दें। और चूँकि एसडीजी के पीछे कोई ठोस सिद्धांत नहीं है और इनकी प्रगति के लिए सिर्फ़ क़र्ज़ लेना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए एसडीजी को छलावा की तरह ज़्यादा और असलियत की तरह कम इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तविकता एसडीजी 17.4 के विपरीत है, जो ‘ऋण वित्तपोषण, ऋण राहत और ऋण पुनर्गठन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समन्वित नीतियों के माध्यम से विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करना’ है।5 दूसरे शब्दों में कहें तो एसडीजी के काम सिर्फ़ धन की कमी की वजह से ही नहीं रुके हुए हैं, जैसा कि इसके विरोधियों का कहना है। बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था और विकास के कार्यक्रम की वजह से भी रुके हैं जो [वैश्विक] दक्षिण को अविकसित देखना चाहती है और साथ ही इस अवस्था से उबरने के लिए वैश्विक दक्षिण के पास एक वैकल्पिक विकास सिद्धांत और कार्यक्रम भी नहीं है।
एसडीजी की रूपरेखा तैयार होने और यूएन के सभी सदस्यों के इसे अपना लेने के तीन साल बाद 2018 में ही आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ताओ चांग ने लिखा कि 40% कम आय वाले देशों पर क़र्ज़ से जुड़ा भारी संकट है – 2015 में एसडीजी पारित होने के समय यह आँकड़ा 26% था – इसलिए वे ऋण नहीं चुका पा रहे हैं।6 यूएन के सतत विकास के लिए वित्तपोषण रिपोर्ट 2024 में दिखाया गया कि सबसे ग़रीब विकासशील देशों पर औसत ऋण का बोझ 2023 में बढ़कर 12% हो गया, ‘जोकि सन् 2000 के बाद का उच्चतम स्तर है’।7
वैश्विक दक्षिण के लिए विकास का एक नया सिद्धांत गढ़े जाने की सख़्त ज़रूरत है। एक ऐसा सिद्धांत जो एसडीजी जैसे प्रयासों के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों या आईएमएफ और इसके ऋण-मितव्ययिता के राज के असफल तरीक़ों से आगे जाए। विकास के एक वैज्ञानिक सिद्धांत के बिना कोई भी विकास कार्यक्रम बन ही नहीं सकता।8 यह डोसियर ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान और ग्लोबल साउथ इन्साइट्स ने मिलकर तैयार किया है। यह नवउदारवाद के विकास के असफल सिद्धांतों और वैश्विक दक्षिण के लिए विकास के नए सिद्धांत को विकसित करने की ज़रूरत से जुड़ी बहस को सामने रखता है। इसके साथ यह वैश्विक दक्षिण के लिए विकास के एक नए सिद्धांत की शुरुआती रूपरेखा भी पेश करता है। अगले कुछ सालों में विकास के नए सिद्धांत पर इसी तरह के और दस्तावेज़ निकाले जाएंगे जो ख़ास देशों और क्षेत्रों के अध्ययन पर और व्यापक सम्भावनाओं पर आधारित होंगे।
अल्पविकास के सिद्धांत
इससे पहले कि हम विकास के नए सिद्धांत के ख़ास बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें यह ज़रूरी है कि हम विकास के दूसरे नज़रियों पर निगाह डालें, जैसे आधुनिकता का सिद्धांत (जो डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्तोव के विचारों से प्रचलित हुआ), वॉशिंगटन कॅन्सेंसस और निर्भरता के सिद्धांत जैसे अन्य परिवर्तनकामी सिद्धांत तथा इनकी वजह से वामपंथ में उभरे विमर्श।
आधुनिकता का सिद्धांत
अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों, लिंडन जॉनसन और जॉन एफ़. केनेडी के समाजवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता विरोधी अभियानों में सलाहकार रहे अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्तोव ने 1960 में द स्टेजेस ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ: ए नॉन-कम्युनिस्ट मैनिफ़ेस्टो (आर्थिक विकास के चरण: एक ग़ैर–कम्युनिस्ट घोषणापत्र) नामक एक किताब लिखी। इसके शीर्षक से ही इसकी मंशा ज़ाहिर हो जाती है। रोस्तोव वैचारिक रूप से पक्के कम्युनिस्ट विरोधी और शीत युद्ध समर्थक थे। उन्होंने विकास का एक सार्वभौमिक और एकरेखीय प्रक्रिया का सिद्धांत पेश किया जो तथाकथित ‘पारम्परिक समाज’ को ‘उड़ान की पूर्वावस्था’ (preconditions for take-off) तक ले जाए, वहाँ से ‘उड़ान की अवस्था’ (take-off) तक, फिर ‘परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था’ (drive to maturity) तक और अंतत: ‘जन उपभोग की अवस्था’ (age of mass consumption) तक।9 उनका मत था कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एक ऐसे उद्यमी वर्ग को जन्म देगी जो तर्कशून्य परम्पराओं की बजाय ‘तर्कसंगत’ आर्थिक प्रोत्साहनों को तरजीह देगा। उनका मत था कि इससे निवेश की दरें ऊँची होंगी तथा आर्थिक विविधता बढ़ेगी जिसकी परिणति काफ़ी हद तक एक ऐसे उपभोक्तावादी समाज में होगी जिसे वैश्विक उत्तर में पहले ही हासिल किया जा चुका है।
रोस्तोव का सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आधुनिकता के विचारों का एक मिलाजुला नमूना था जो सेंट लशिया के अर्थशास्त्री डब्ल्यू. आर्थर लुईस जैसे लोगों का अनुसरण करता है। यह सिद्धांत कहता है कि आर्थिक विकास तभी होगा जब बेशी श्रम/श्रमिक ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर मुख्यतः शहरी और औद्योगिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाएँगे।10 रोस्तोव और आधुनिकता के अन्य सिद्धांतकारों ने विकास को पूँजीवाद की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने यह भारी ग़लती अपने अनैतिहासिक सोच की वजह से की जो यह मानकर चलती है कि पाँच सौ वर्षों के उपनिवेशवादी शासन के बाद वैश्विक दक्षिण उसी बिंदु से शुरुआत कर रहा था जहाँ औद्योगिक क्रांति से पहले का यूरोप खड़ा था। उन्होंने अल्पविकास को एक मौलिक घटना समझ लिया। जबकि असल में वैश्विक दक्षिण में कोई ‘पारम्परिक समाज’ जैसी चीज़ थी ही नहीं। बल्कि वहाँ एक सर्वथा नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था थी जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने जबरन और हिंसक तरीक़े से लागू की थी। और तो और, औद्योगिक क्रांति से पहले के यूरोप से उलट वैश्विक दक्षिण एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहाँ वैश्विक उत्तर का तकनीक, व्यापार और वित्तीय व्यवस्था पर एकाधिकार था। इस दुनिया में एक नवउपनिवेशवादी आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा भी पहले से ही काम कर रहा था।
रोस्तोव की यह सोच उनके पिछले शोध जैसे ऐन अमेरिकन पॉलिटिक्स इन एशिया (1955, सहलेखक रिचर्ड डब्ल्यू. हैच) पर आधारित है जिसमें शीत युद्ध के संदर्भ में आधुनिकता शीत युद्ध के संदर्भ पर ज़्यादा खुलकर चर्चा मिलती है। ऐन अमेरिकन पॉलिटिक्स में रोस्तोव लिखते हैं कि ‘संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से छेड़े गए सम्पूर्ण युद्ध का विकल्प शांति नहीं है। जब तक मॉस्को और पेकिंग [sic] में एक अलग भावना और अलग नीति नहीं लागू होगी तब तक अमेरिका के सामने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों का प्रयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।’11 दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वह ‘सम्पूर्ण युद्ध’ (जिसमें विजय के लिए हर सम्भव प्रयास और बलिदान दे दिया जाए) सहित अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल सोवियत यूनियन और चीन के जनवादी गणराज्य से कम्युनिज़्म को उखाड़ फेंकने के लिए करे। रोस्तोव जैसे सिद्धांतकारों के लिए साम्यवाद के ख़िलाफ़ युद्ध पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत यह समझना कि इससे बहुमूल्य मानव श्रम ज़ाया होगा। कोई हैरानी नहीं कि 60 के दशक में राजनीति वैज्ञानिक सैम्यूअल हंटिंगटन ने ‘सैन्य आधुनिकता’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें तहत दो बातें कही गईं, पहली कि तीसरी दुनिया के देशों में ‘सामाजिक आधुनिकता’ हासिल करने का सबसे अच्छा तरीक़ा होगा इन देशों का सैन्यीकरण किया जाना, और दूसरी, इसका नतीजा यह हुआ कि कम्युनिज़्म से लड़ने और अमेरिका जैसे ‘आधुनिक समाज’ के निर्माण के लिए सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।12
50 और 60 के दशकों में आईएमएफ और विश्व बैंक के लिए विकास के आदर्श की परिभाषा आधुनिकता का सिद्धांत बन गया। जब यह सिद्धांत तीसरी दुनिया को ‘उड़ान की अवस्था’ में पहुँचाने में असफल हो गया तब भी सत्ता के गलियारों में इसकी साख कम नहीं हुई। यूएस डॉलर के स्थिर और अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर निर्भर देशों पर जब तीसरी दुनिया के ऋण संकट की मार पड़ी तब इसका प्रभाव कम हुआ। जब 1979 में यूएस फ़ेडरल रिज़र्व ने जल्दी-जल्दी ब्याज दर बढ़ाई तो विकासशील देशों को ऋण मिलने में मुश्किल हुई और इससे कई ख़तरनाक आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं (इसमें 1982 में मेक्सिको का दिवालिया हो जाना भी शामिल है)।13 आधुनिकता का सिद्धांत पेसो (मेक्सिको की मुद्रा) के साथ ढह गया और आईएमएफ तथा विश्व बैंक का काम आगे बढ़ाने के लिए एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ।
द वॉशिंगटन कॅन्सेंसस
नब्बे के दशक में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और पीटर्सन इन्स्टिट्यूट फ़ॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सीनियर फ़ेलो जॉन विल्यम्सन ने सरकारी उद्यमों (state-owned enterprises, SOE) के निजीकरण, सार्वजनिक उत्पादों को कॅमोडिटी में बदलने और पूंजी अकाउंट तथा व्यापार के उदारीकरण को परिभाषित करने के लिए वॉशिंगटन कॅन्सेंसस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया।14 अमेरिकी ट्रेज़री के हिसाब से IMF और विश्व बैंक की इस नीति को अपना सैद्धांतिक आधार नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र और फ़्रीड्रिक हाइक जैसे विचारकों तथा नवउदारवादी मांट पेलेरीं सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों में मिला।15 वॉशिंगटन कॅन्सेंसस शायद सबसे ज़्यादा तथाकथित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programmes, SAP) में अपनी भूमिका के लिए मशहूर है जिसकी वजह से अफ्रीकी महाद्वीप ने अपना एक दशक खो दिया।16
पिछले कई दशकों से आईएमएफ उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए देशों पर मितव्ययिता (जिसे वे ‘संतुलित बजट’ एजेंडा कहते हैं), निजीकरण और व्यापार के उदारीकरण की नीतियों को थोपता आ रहा है। इसने वैश्विक दक्षिण के देशों से उनकी अपनी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अपेक्षाकृत नए उद्योगों को बचाने की क्षमता छीन ली। इसकी वजह से जो असंतुलन पैदा हुआ उससे निपटने के लिए आईएमएफ ने लगातार विकासशील देशों को निजी पूंजी बाज़ारों से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वे क़र्ज़ के जाल में फँसते चले गए। इस बीच वैश्विक दक्षिण के लिए विश्व बैंक के एजेंडे में बड़े स्तर पर औद्योगीकरण किए जाने का सुझाव कभी आया ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शुरुआती दौर में यही बात स्पष्ट दिखती है जब विश्व बैंक ने इन देशों को कच्चा माल निर्यात करने के अपने ‘तुलनात्मक सुलाभ’ (Comparative Advantage) काम से ही जुड़े रहने की सलाह दी। 90 के दशक तक आते-आते विश्व बैंक ‘वित्तीय गहनता’ को बढ़ावा देने लगा, यह और कुछ नहीं बल्कि विकास के लिए संसाधन जुटाने के रामबाण के रूप में वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना है।17 हाल के समय में विश्व बैंक ने अपना ध्यान सेवा क्षेत्र में विकास और लघु तथा मध्यम उद्योगों (SMEs) में निवेश को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित कर दिया है, दोनों का ही मतलब है कि राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर ऋण का जाल कसता जाएगा। सेवा क्षेत्र में अधिकतर बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों (MNCs) का वर्चस्व होता है जिनकी आधारभूत संरचना ही इजारेदारी पर टिकी होती है। इसकी वजह से जो राष्ट्र अपने विकास का आधार सेवा क्षेत्र को बनाएँगे वे हमेशा ही वैश्विक उत्तर के बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों के भरोसे रह जाएँगे। SMEs के पास बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों का मुक़ाबला करने लायक संसाधन (इसमें सरकारी सब्सिडी भी शामिल है) नहीं होते और न ही वे बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों जितने बड़े होते हैं। इस कारण प्रभुत्वशाली बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन उनको निगल जाते हैं। वित्तीय उदारीकरण और SMEs को बढ़ावा देने की वजह से देश ऐसी स्थिति में फँस जाते हैं जिसे समीर अमीन ने सामान्यीकृत इजारेदारी पूँजी (generalised monopoly capital) का नाम दिया, जो ऊपर की ओर जाने वाले (कच्चा माल, तकनीक और पूँजी) तथा नीचे की ओर जाने वाले (वितरण, मार्केटिंग और उपभोक्ता तक पहुँच) दोनों नेटवर्कों पर नियंत्रण रखती है।18
वॉशिंगटन कॅन्सेंसस का एक प्रमुख नतीजा यह रहा कि आर्थिक प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की ताक़त पर आँख मूँदकर भरोसा किया जाने लगा। FDI से जुड़ी इस सोच ने वैश्विक दक्षिण के देशों को एक संकीर्ण उद्देश्य तक सीमित कर दिया जिसमें उन्होंने अपने श्रम और प्राकृतिक संसाधनों के बाज़ार को पश्चिमी इजारेदारों के लिए खोल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एजेंडे को अपने लोगों की विकास की आकांक्षाओं से जोड़ने की बजाय क़र्ज़ देने वालों की ब्याज़खोर ज़रूरतों से जोड़ दिया। जबकि इस बात के प्रमाण कम ही हैं कि FDI के आने से बहुत बदलाव आते हैं: इस तरह के निवेश से ऐसा सम्पूर्ण विकास नहीं होता जो क़र्ज़ मुक्ति और राष्ट्रीय संप्रभुता के रास्ते खोल सके, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के निरर्थक क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। FDI के निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
- FDI प्रवाह में गिरावट आ रही है। 2007 में FDI अपने चरम पर पहुँचा। इसी साल प्रमुख पूँजीवादी देशों को तीसरी आर्थिक महामंदी ने अपने चंगुल में ले लिया और तब से FDI में लगातार गिरावट आई है।19 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के मुताबिक़ FDI और योजनाओं के लिए वित्तीय निवेश (दीर्घकालिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर या उद्योगों के लिए निवेश) दोनों में निरंतर गिरावट आई है। मसलन 2022 से 2023 के बीच विकासशील देशों में FDI में 7% की गिरावट आई।20
- FDI का प्रवाह अनुत्पादक रहा है। पिछले कुछ सालों में UNCTAD के सालाना निवेश आँकड़ों में FDI के चरित्र में आए बदलाव दिखायी देते हैं। पहले यह मैन्युफ़ैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रित होता था और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के खनन पर भी। लेकिन अब FDI काफ़ी हद तक वित्तीय और सेवा क्षेत्र में जा रहा है जहाँ यह ऐसे सम्पूर्ण या बदलाव लाने वाले विकास को जन्म नहीं देता जो उपनिवेशवादी काल के अल्पविकास से उबार पाए।
- FDI प्रगति या निवेश को बढ़ावा नहीं देता। UNCTAD की 1999 की रिपोर्ट के मुताबिक़ 90 के दशक में विकासशील देशों में बड़े स्तर पर हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने निवेश के पैटर्न पर बहुत कम प्रभाव डाला।21 UNCTAD के हाल के अध्ययनों में साफ़ दिखता है कि तीसरे आर्थिक महाअवसाद के बाद से FDI प्रवाह और GDP संवृद्धि अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं।22 इसका मतलब है कि आर्थिक विकास FDI पर निर्भर नहीं करता है।
वॉशिंगटन कॅन्सेंसस ने उपनिवेशवादी दौर के अल्पविकास के पैटर्न को ही फिर से लागू कर दिया है जिसकी वजह से क़र्ज़ का बोझ इतना बढ़ गया है जो चुकाया नहीं जा पा रहा। निवेशक क़र्ज़ लेने वाले देशों की आर्थिक दशा को नज़रंदाज़ करते हुए बकाया और ब्याज वसूली पर आमादा हैं। क़र्ज़ का यह कुचक्र वह सारी आय निगल जाता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और उत्पादक उद्योगों तथा इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। देश बस क़र्ज़ लेते हैं और उसमें डूबते चले जाते हैं। जब वो मौजूदा क़र्ज़ चुका नहीं पाते तो इसे चुकाने के लिए और क़र्ज़ लेते हैं और इस तरह एक कुचक्र चलता रहता है।23 2003 से 2007 तक आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे रघुराम राजन ने अपनी किताब फॉल्ट लाइन्स (2010) में लिखा, आईएमएफ की नीतियाँ ‘वित्तीय उपनिवेशवाद का एक नया रूप’ है।24
निर्भरता सिद्धांत
निर्भरता सिद्धांत आधुनिकता सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ और इसका एक लम्बा तथा प्रभुत्वशाली इतिहास है। इसकी जड़ें लैटिन अमेरिका के संरचनावाद और राउल प्रीबिश जैसे दिग्गजों तथा अन्य निर्भरता सिद्धांतकारों (dependencistas) के काम में देखी जा सकती हैं, जिनका मत था कि दुनिया की पूँजीवादी व्यवस्था दो स्तरों से बनी है: पहला, उन देशों का छोटा सघन समूह जिनका दुनिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व है, तथा दूसरा स्तर, हाशिए के देशों का बड़ा समूह जो इस सत्ता से छूट पाने में असमर्थ हैं। जैसा कि निर्भरता सिद्धांतकारों ने दिखाया, औद्योगिक क्षमता वाले देशों के छोटे समूह और हाशिए पर धकेल दिए गए वे देश जो औद्योगिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इनके बीच व्यापार की ख़राब शर्तों की वजह से हाशिए के देशों में अल्पविकास और अस्थिरता पैदा हुई।25 हाशिए के देश ज़्यादातर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो प्रासेस्ड नहीं होतीं, जिन्हें कम दामों पर ख़रीदा जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ज़रिए औद्योगिक रूप से विकसित देशों को बेचा जाता है, जो अपनी औद्योगिक क्षमता से इसे पक्के माल में तब्दील करते हैं, फिर यही महँगी वस्तुएँ वापस हाशिए के देशों में बेची जाती हैं। इस छोटे विकसित समूह और हाशिए के देशों के बीच जिन शर्तों पर व्यापार होता है उसने इस विकसित देशों के समूह में पूँजीवादी संचय का होना संभव बनाया। इसका इस्तेमाल नए उत्पादों और तकनीक के आविष्कार के लिए किया गया। इसी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के सहारे औद्योगिक क्षमता वाले देशों के गुट पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसे आंद्रे गंडर फ़्रैंक ने ‘अल्पविकास का विकास’ कहा है, एक निराशाजनक वास्तविकता का नकारात्मक विश्लेषण।26
निर्भरता सिद्धांत ने बिलकुल साफ़ कर दिया कि यह निराशाजनक वास्तविकता तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से नहीं उपजी है बल्कि उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी दौर में जो नवउपनिवेशवादी व्यवस्था स्थापित हुई उससे निकली है। इसीलिए 1972 में प्रकाशित वॉल्टर रॉड्नी की क्लासिक किताब का शीर्षक है हाऊ यूरोप अंडरडेवल्पड अफ्रीका [यूरोप ने कैसे अफ़्रीका को अल्पविकसित बनाया], जिसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद पर ख़ास ध्यान दिया गया।27 जैसा कि गंडर फ़्रैंक ने समझाया ‘अल्पविकास कोई मौलिक परिस्थिति नहीं है, यह विकसित महानगरीय पूँजीवाद द्वारा पिछड़े क्षेत्रों पर आर्थिक क़ब्ज़े और नियंत्रण से पैदा होती है’।28
इस सिद्धांत से निकली नकारात्मक्ता से ही समीर अमीन के इस मत को विकसित किया कि हाशिए के देशों को औद्योगिक रूप से विकसित देशों के समूह से ‘अलग’ होना होगा। अमीन ने 1987 में लिखा कि इस अलग होने का मतलब ‘राष्ट्रीय विकास की रणनीति को “भूमंडलीकरण” की अनिवार्यताओं के आगे समर्पित कर देने की अस्वीकृति’ है।29 चूँकि इस ‘अस्वीकृति’ की जड़ें राजनीतिक ताक़त में हैं और आर्थिक नीति में उतनी नहीं इसलिए विकासशील दुनिया के देशों के पास इतनी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए कि वे अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीति ख़ुद तैयार कर सकें और वैश्विक मूल्य चेन (जिसे बेंजामिन सेल्वन ने ‘वैश्विक ग़रीबी चेन’ का सटीक नाम दिया) की दासता से मुक्त हो सकें या ‘अलग’ हो सकें।30
निर्भरता सिद्धांत की आलोचनाएँ
निर्भरता सिद्धांत विकास के एक नए सिद्धांत की ज़रूरत का तो बहुत सटीक विश्लेषण करता है लेकिन ख़ुद ऐसा कोई नया सिद्धांत पेश नहीं करता। दूसरे शब्दों में निर्भरता सिद्धांत सिर्फ़ नवउपनिवेशवादी व्यवस्था की आलोचना और राष्ट्रीय विकास रणनीति के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए अलग होने की ज़रूरत तक ही ख़ुद को सीमित कर लेता है, लेकिन विचार की यह परंपरा – जो कि हमारी परंपरा भी है – कोई ऐसी रणनीति या योजना सामने नहीं रखती जो ये बदलाव ला सके।31
प्रगतिशील और मार्क्सवादी आर्थिक सोच रखने वालों के बीच निर्भरता सिद्धांत की आलोचना तीन प्रमुख विचारों पर देखी जा सकती है।
पहला, कुछ परिवर्तकामी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि एशियन टाइगर्स कहे जाने वाले चार एशियाई देशों (हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान) के उत्थान ने निर्भरता सिद्धांत के औचित्य को ही नकार दिया है और यह दावा भी किया कि व्यावहारिक मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ राज्य के समन्वित हस्तक्षेप द्वारा पूँजीवादी अल्पविकास की जड़ता से उबरा जा सकता है। एशियन टाइगर्स की परिघटना में दिलचस्पी ने विकासात्मक राज्य और औद्योगिक नीति पर एक नए विचार के पूरे साहित्य की ही शुरुआत कर दी। इस संदर्भ में बुनियादी किताबें हैं जॉनसन कामर की MITI and the Japanese Miracle (1982) और ऐलिस ऐम्स्डन की Asia’s Next Giant (1989)।32 विश्व बैंक ने भी इससे जुड़ी The East Asian Miracle (1993) नाम से एक लंबी रिपोर्ट निकाली, हालाँकि इसके विश्लेषण में राज्य की भूमिका को कमतर करके दिखाए जाने का प्रयास किया गया।33 इसमें कोई शक़ नहीं कि हा-जून छांग और मारीयाना मज़्ज़ुकटो जैसे हस्तियों ने भी वैश्विक दक्षिण में सेंटर-लेफ़्ट सरकारों के लिए लोगों को प्रभावित किया है।34 फिर भी इनके विचार पुराने उदाहरणों पर आधारित एक शासन चलने की एक रणनीति भर का प्रस्ताव देते हैं और विकास का एक नया सिद्धांत या पूरे वैश्विक दक्षिण की विभिन्न वास्तविकताओं को अपने विश्लेषण में जगह देने में असफल रहे। जहाँ चार एशियन टाइगर्स शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सुरक्षा में विकसित हुए, वहीं अफ़्रीकी, लैटिन अमेरिकी या अन्य एशियाई देशों को नवउदारवादी हस्तक्षेपों या साम्राज्यवादी और पूँजीवादी दायरों में अपना विकास करना पड़ा।35
दूसरा, ब्रिटिश विचारक बिल वॉरन जैसे कुछ मार्क्सवादी सक्रिय रूप से साम्राज्यवाद के तथाकथित प्रगतिशाली पहलुओं के पक्ष में मत रखते रहे। अपनी किताब Imperialism: Pioneer of Capitalism (1980) में वॉरन ने लिखा कि वैश्विक दक्षिण के पिछड़े देशों के आधुनिकीकरण में साम्राज्यवाद एक परिवर्तनकारी ऊर्जा की भूमिका निभा सकता है क्योंकि उनके मुताबिक़ यह औद्योगीकरण और लोकतंत्र दोनों की नींव रखता है।36 वॉरन ने जो साम्राज्यवाद को कथित वामपंथी जामा पहनाने की कोशिश की उसकी वैश्विक दक्षिण के मार्क्सवादी-लेनिनवादियों ने बहुत आलोचना की क्योंकि वे जानते थे कि कैपिटल इन मोशन (पूँजी की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही) के रूप में साम्राज्यवाद न सिर्फ़ [वैश्विक] दक्षिण की उत्पादन शक्तियों के विकास में विफल रहा है: साथ ही साथ इसने इनकी अर्थव्यवस्थाओं को बेहद अल्पविकसित रखा, इनके संसाधनों को लूटा और बर्बर युद्धों, शोषण और उत्पादन की स्थानीय व्यवस्थाओं को बर्बाद करके इन देशों को दूसरों पर निर्भर बना दिया।37 वॉरन का सिद्धांत नवक्लासिकीय आधुनिकता सिद्धांत के ही एक रूप के अलावा और कुछ नहीं था जो मार्क्सवादी शब्दों में लिखा गया था।
तीसरा, 70 और 80 के दशकों में राजनीतिक मार्क्सवादी कहे जाने वाले कुछ मार्क्सवादियों ने निर्भरता सिद्धांतकारों पर ‘नव-स्मिथवादी मार्क्सवादी’ होने का आरोप लगाया कि इन्होंने विकसित देशों के छोटे समूह और हाशिए के देशों के व्यापारिक संबंधों पर अत्यधिक ध्यान दिया जबकि हाशिए के देशों के आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को नज़रंदाज़ कर दिया।38 इसके बावजूद नव-स्मिथवादियों और राजनीतिक मार्क्सवादियों के बीच समझौते की कुछ कसर रहती है, क्योंकि कुछ सिद्धांतकर्ताओं ने साम्राज्यवादी रिश्तों जैसे बाहरी कारणों को वर्गीय संबंधों जैसे आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक पारस्परिक व्यवहारों को आपस में जोड़ने के प्रयास किए।
श्रीलंकाई मार्क्सवादी अर्थशास्त्री एस. बी. डी. डी. सिल्वा ने अपनी बेहतरीन किताब The Political Economy of Underdevelopment (1982) में कहा कि साम्राज्यवाद ने व्यापारिक पूँजी को विकसित और मज़बूत किया जबकि औद्योगिक पूँजी को कमज़ोर।39 डी सिल्वा का मानना था कि इस बात पर बहस करने की बजाय कि हाशिए के देश पूँजीवादी हो चुके हैं या नहीं (निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना था कि ऐसा हो चुका जबकि रॉबर्ट ब्रेनर जैसे राजनीतिक मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते थे) से बेहतर होगा यह अध्ययन करना कि साम्राज्यवाद ने कैसे आंतरिक वर्गीय संरचना के ज़रिए उन तत्वों को बढ़ावा दिया जो औद्योगीकरण के ख़िलाफ़ थे। डी सिल्वा के अनुसार अल्पविकास एक ऐसे वर्गीय और आर्थिक ढाँचे की अनुपस्थिति से जुड़ा हुआ था जो न सिर्फ़ धन के स्तर पर पूँजी संचय करता है बल्कि उत्पादक स्थाई संपत्ति के स्तर पर भी।
इसी तरह पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के समाजवादी धड़ों के विचारकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवउपनिवेशवादी निर्भरता और वैश्विक दक्षिण की अंदरूनी वर्गीय संरचना की भूमिका का अपना अलग विश्लेषण विकसित किया। उदाहरण के लिए सोवियत राजनीतिक अर्थशास्त्री सेर्गे ट्यूलपनोव का मत था कि राज्य को उन घरेलू शक्तियों को अलग-थलग करना होगा जो औद्योगीकरण में रुकावट पैदा कर रही हैं (ज़मींदार और व्यापारिक पूँजी) तथा एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा करना होगा, साथ ही निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय बुर्जुआ की प्रगतिशील भावी संभावनाओं को प्रेरित करना चाहिए।40 इस ‘ग़ैर-पूँजीवादी विकास’ की रणनीति के तहत यह ज़रूरी है कि राष्ट्रीय-लोकतांत्रिक दलों को नेतृत्व का भार उठाना होगा और बुर्जुआ के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं देनी होगी।
विकास का एक मार्क्सवादी सिद्धांत
पिछले पचास सालों में, वॉशिंगटन कॅन्सेंसस जब अपने चरम पर था, अधिकतर ग़रीब देश ऋण और ख़र्चों में कटौती के कुचक्र, ग़रीबी की ऊँची दर और गहरी निराशा में डूब गए। लेकिन चीन 1949 की क्रांति के बाद से ‘अल्पविकास के विकास’ के दौर से बाहर निकल पाया है और ग़रीबी की ऊँची दर को कम करके एक ऐसे समाज की ओर बढ़ पाया है जिसने अति-ग़रीबी को ख़त्म कर दिया है और एक बड़ी आर्थिक ताक़त के रूप में उभरा है।41 चीन और बाक़ी देशों में अंतर यह है कि यहाँ राजनीतिक सत्ता का संतुलन पूँजीपति वर्ग (ख़ासतौर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) के हाथों में नहीं है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाई जा रही चीनी सरकार ने योजना की एक प्रक्रिया विकसित की है जो द्वंद्वात्मक संतुलन बनाते हुए संसाधनों का वितरण विकास और सामाजिक बेहतरी दोनों के लिए करती है। किसी भी ठोस और व्यावहारिक विकास के मार्क्सवादी सिद्धांत को चीन की सफलताओं को समझना होगा। इस संदर्भ में दो बिंदुओं को उजागर करना ज़रूरी है।
पहला, हालाँकि चीन में पूँजीवादी वर्ग है लेकिन राजनीतिक सत्ता पर इसका प्रभुत्व स्थापित नहीं होने दिया गया है। वैश्विक उत्तर के समाजों में जो पारस्परिक संबंध मौजूद हैं – जहाँ राज्य और अन्य संस्थान निजी पूँजी के इशारों पर चलते हैं – वे चीन में नहीं हैं, यहाँ ये संस्थान राजनीतिक सत्ता द्वारा संचालित हैं जो समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही चीन में एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें भूमि, वित्त, व्यापार और बड़े उद्योग शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि चीन में आर्थिक निर्णयों पर मूल्य के पूँजीवादी नियम को हावी नहीं होने देता। इसलिए चीन के प्रयोग आधुनिकता के सिद्धांत के साँचे में नहीं ढलते।
दूसरा, चूँकि राजनीतिक सत्ता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है इसलिए यहाँ राजनीतिक निर्णय दूसरे देशों या इकाइयों के हितों के आधार पर नहीं होते (जैसा कि वॉशिंगटन कॅन्सेंसस में दिखा)। जैसा कि अमीन ने कहा कि चीन ख़ुद को ‘अलग’ कर पाने में सफल रहा जिससे यह राष्ट्रीय विकास की रणनीति अपनी विकासात्मक नीति के आधार पर व्याख्यायित कर पाया।42 यह हासिल किया गया देश की ज़मीन और वित्त पर सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण द्वारा जिससे राज्य व्यापार, निवेश और वैश्विक मूल्य की श्रृंखला के ज़रिए विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा, इससे श्रम का समाजीकरण हुए (जो मार्क्स की समाजवाद की राजनीतिक दृष्टि का एक अहम हिस्सा है)। इससे चीन निर्भरता सिद्धांत की नकारात्मकता से निकल पाया और दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक देश बन पाया।
आधुनिकता और निर्भरता दोनों ही सिद्धांत चीन के उत्थान को पूरी तरह नहीं समझा पाते। चीन में एक विकासात्मक देश के कुछ पहलू दिखाई देते हैं जैसे सक्रिय औद्योगिक नीतियाँ, लेकिन इनके आधार पर इसके तीव्र विकास की सैद्धांतिक व्याख्या हमें नहीं मिल पाती। चीन का सुधार और खुलापन (1978) एक पुनरावृत्तीय और प्रायोगिक प्रक्रिया थी, जो हमेशा स्थानीय परिस्थितियों के महत्व पर जोर देती थी। हालाँकि यह अब तक एक विकसित अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित नहीं हुआ है लेकिन जैसा कि एनफ़ू छंग और छान त्ज़ाय का मत है चीन ने ‘समृद्धि की तरफ़ लगातार बढ़ते रहने की स्थिति’ को हासिल कर लिया है, यह हाशिए के देशों से निकलकर वैश्विक व्यवस्था के ‘अर्द्ध-केंद्रीय’ स्थान तक आ चुका है।43
इस स्थिति में भी चीन अति-ग़रीबी को ख़त्म करने में सफल हो पाया है और विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में बहुत अहम प्रगति कर पाया है। इसके पीछे क्या ख़ास वजह हैं? हमारे विकास के नए सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक और शुरुआती बिंदु यह होना चाहिए कि चीन के आर्थिक मॉडल में निवेश और जीडीपी का अनुपात निरंतर ऊँचा रहा है जिससे इन्फ़्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षमता के रूप में बहुत अधिक स्थाई पूँजी का निर्माण हुआ।
ग्लोबल साउथ इन्साइट्स (जीएसआई) के नए शोध से पता चलता है कि जीडीपी वृद्धि की उच्च मात्रा और स्थाई पूंजी निर्माण की उच्च हिस्सेदारी के बीच एक अति-उच्च सहसंबंध है, जिसे हम संक्षेप में शुद्ध स्थाई निवेश (एनएफआई) कहते हैं। शुद्ध स्थाई निवेश का मतलब है नया स्थाई पूँजी निवेश (मसलन किसी अवधि के दौरान मशीनों, इन्फ़्रास्ट्रक्चर इत्यादि के निर्माण पर हुए कुल खर्च में से इस दौरान ख़राब अथवा बेकार हुए मौजूदा पूँजी स्टॉक को घटाकर सकल स्थाई निर्माण की गणना की जाती है)। संक्षेप में, जीडीपी में शुद्ध स्थाई निवेश की हिस्सेदारी जितनी ज़्यादा रहेगी विकास की दर भी उतनी ऊँची रहेगी। यह उच्च सहसंबंध उन 50 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती है जो दुनिया की जीडीपी का 88% बनाते हैं। यह वैश्विक दक्षिण की 50 से ज़्यादा छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर भी लागू होता है।44 मतलब यह कि सिर्फ़ वित्तीय निवेश का आना ही काफ़ी नहीं है बल्कि जीडीपी के विकास के लिए ठोस परिसंपत्तियों में निवेश भी ज़रूरी है।
जीडीपी आर्थिक विकास मापने का एक अपूर्ण परिमाण है क्योंकि यह पर्यावरण के नुक़सान और सामाजिक विकास के तत्वों जैसे ‘बाह्य कारकों’ को नहीं गिनता। इसका मतलब यह नहीं कि जीडीपी ग़ैर-ज़रूरी है। ग्लोबल साउथ इन्साइट्स के शोध ने प्रति व्यक्ति जीडीपी और जीवन प्रत्याशा के बीच एक अहम और मज़बूत सहसंबंध पाया है। यह सहसंबंध 90 के दशक से लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोत्तरी और कम आय वाले वर्गों के लोगों की जीवन प्रत्याशा में अनुपातिक वृद्धि में भी सहसंबंध है। दूसरे शब्दों में, जीडीपी के विकास से वैश्विक दक्षिण के लोगों के जीवन में बहुत वास्तविक भौतिक बदलाव आ सकते हैं। दूसरी ओर, जीडीपी विकास में ठहराव, जैसा कि तीसरी दुनिया के देशों में ऋण संकट और नवउदारवाद की शुरुआत की वजह से हुआ, दशकों तक ऐसा समय ला सकता है जब मानव विकास के संदर्भ में बहुत कम या नगण्य प्रगति होती है। ज़ाहिर है सामाजिक सुरक्षा की भी एक अहम भूमिका है: इस संदर्भ में कई बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं जैसे समाजवादी क्यूबा जिसने अमेरिका द्वारा छ: दशक के प्रतिबंध की वजह से तीव्र गति से आर्थिक प्रगति न होने के बावजूद ऊँची जीवन प्रत्याशा दर हासिल की।
जबकि हमें पता है कि NFI और जीडीपी विकास में सकारात्मक संबंध है और प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास और जीवन प्रत्याशा दर में भी सकारात्मक संबंध है, तो वैश्विक दक्षिण की प्रगतिशील सरकारों के लिए बुनियादी काम यह है कि वे जीडीपी में NFI की हिस्सेदारी को बढ़ाएँ। लेकिन इसमें तीन चुनौतियाँ खड़ी होती हैं:
- NFI का जीडीपी में हिस्सा इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि कुछ समय के लिए यह माँग को असह्य स्तर तक गिरा दे। इसके लिए ऐसे मददगार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की ज़रूरत है जो NFI के लिए रियायती और दीर्घावधि वित्तीय मदद दे सकें।
- ऐसे तंत्रों की ज़रूरत है जो वैश्विक दक्षिण से संपदा की लूट को रोक सकें और उन्हें NFI के विकास में लगा सकें। इसके लिए कर की चोरी, ट्रान्स्फ़र प्राइसिंग और व्यापार में ग़लत बिल बनाने जैसे कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य की ज़रूरत है। इसके साथ ही वस्तुओं के दाम स्थिर करने के लिए बहुस्तरीय तंत्रों की भी ज़रूरत है।
- NFI उत्पादक और पर्यावरण के नज़रिए से उचित होना चाहिए (यानी अच्छे स्तर का)। यह स्पष्ट है कि रियल इस्टेट जैसे सट्टे के क्षेत्रों में NFI के वे परिणाम नहीं होते जो इन्फ़्रास्ट्रक्चर, खेती और आधुनिक उद्योगों जैसे उत्पादक क्षेत्रों में NFI के होते हैं। उत्पादक क्षेत्र स्किल, तकनीक के संचय के लिए और भौतिक पदार्थों के उत्पादन के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही आवास और आवास से जुड़े इन्फ़्रास्ट्रक्चर में NFI का जीडीपी विकास दर और जीवन प्रत्याशा दर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सबके लिए ज़रूरी है देश के लिए विशिष्ट औद्योगिक और कल्याणकरी नीतियाँ जो तभी तैयार की जा सकती हैं जब हर विशेष मामले में वर्ग संघर्ष की ताक़तों में संतुलन हासिल किया जा सकेगा।
निष्कर्ष
1949 की क्रांति के बाद से चीन के तीव्र आर्थिक विकास और बढ़ते हुए जीवन स्तर को विकास के पारंपरिक सिद्धांतों द्वारा नहीं समझा जा सकता। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा NFI की ऊँची दर को प्राथमिकता देने से ज़रिए इसे समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर, चीन का तेज़ रफ़्तार रेल तंत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा है – के निर्माण के लिए बहुत अधिक निवेश और लोगों को लामबंद करने की ज़रूरत थी। यह कोई नया विचार नहीं था। हालाँकि इस में मतभेद थे कि अर्द्ध-सामंती और साम्राज्यवादी दायरे के भीतर निवेश कैसे इकट्ठा किया जाए, मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचार की परंपरा ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि बड़े स्तर के उद्योग समाजवाद के लिए भौतिक आधार बनाते हैं। 1920 में व्लादिमीर लेनिन ने जोर देते हुए कहा था कि कम्युनिस्ट विकास का मतलब है ‘सोवियत सत्ता और पूरे देश में बिजली पहुँचना’।45 आधी सदी के बाद अफ़्रीकी क्रांतिकारी अमिलकर कब्राल ने हमें सिखाया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य है ‘राष्ट्रीय उत्पादक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया को निर्बाध बनाना’।46 इसलिए वैश्विक दक्षिण के लिए विकास के एक नए सिद्धांत को गढ़ना अपने आप में साम्राज्यवाद और नवउदारवाद से आज़ादी पाने के संघर्षों की ओर लौटना भी है। इसके साथ हम पिछड़े देशों की विराट आकांक्षाओं की राह का नक़्शा तैयार करेंगे।
नोट
1 World Health Organisation, ‘Millennium Development Goals (MDGs)’, 19 February 2018, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs).
2 UN Secretary-General, Progress Towards the Sustainable Development Goals: Towards a Rescue Plan for People and Planet: Report by the Secretary-General, United Nations Digital Library, July 2023, https://digitallibrary.un.org/record/4014344?ln=en&v=pdf, 1–2.
3 United Nations Department of Economic and Social Affairs, ‘UN Chief Urges “Surge in Investment” to Overcome $4 Trillion Financing Gap’, accessed 9 December 2024, https://www.un.org/en/desa/un-chief-urges-%E2%80%98surge-investment%E2%80%99-overcome-4-trillion-financing-gap.
4 Organisation of Economic Co-operation and Development, ‘The 0.7% ODA/GNI Target – A History’, accessed 9 December 2024, https://web-archive.oecd.org/temp/2024-06-17/63452-the07odagnitarget-ahistory.htm; United Nations Economic Commission for Europe, ‘Indicator 17.2.1 (a) Net Official Development Assistance (ODA) as a Percentage of OECD-DAC Donors GNI (Grant Equivalent Methodology), %’, accessed 9 December 2023, https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=72; Henry-Laur Allik, ‘Record Number of NATO Allies to Hit 2% Defense Spending Goal’, Deutsche Welle, 19 June 2024, https://www.dw.com/en/record-number-of-nato-allies-to-hit-2-defense-spending-goal/a-69401037. Our forthcoming publication, The Most Dangerous Organisation on Earth: the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Dossier no. 89, June 2025, will trace the implications to the world of this increase in military spending in the NATO countries.
5 United Nations Conference on Trade and Development, Division on Globalisation and Development Strategies, ‘Target 17.4: Long-Term Debt Sustainability’, accessed 9 December 2024, https://stats.unctad.org/Dgff2016/partnership/goal17/target_17_4.html.
6 Tao Zhang, ‘Managing Debt Vulnerabilities in Low-Income and Developing Countries’, IMF Blog, 22 March 2018, https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/03/22/managing-debt-vulnerabilities-in-low-income-and-developing-countries; International Monetary Fund, ‘Public Debt Vulnerabilities in Low-Income Countries: The Evolving Landscape’, December 2015, https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/110215.pdf.
7 United Nations Inter-Agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2024: Financing for Development at a Crossroads (New York: United Nations, 2024), https://desapublications.un.org/publications/financing-sustainable-development-report-2024, xiv.
8 For more on the formulation of new development theories see Tricontinental: Institute for Social Research, The World Needs a New Socialist Development Theory, dossier no. 66, 4 July 2023, https://thetricontinental.org/dossier-66-development-theory/.
9 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).
10 W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1955).
11 W. W. Rostow and Richard W. Hatch, An American Policy in Asia (Cambridge: MIT Press, 1955), vii.
12 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968). This book was far from the idealistic portrayal of civilian control over the military in Huntington’s The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Boston: Belknap of Harvard University Press, 1957).
13 Cheryl Payer, The Debt Trap: The International Monetary Fund and the Third World (New York: Monthly Review Press, 1974); Leo Panitch and Sam Gindin, ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 41, 2005.
14 John Williamson, ed., Latin American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington, DC: Institute for International Economics, 1990).
15 It is important to note that it was these same thinkers who engineered the neoliberal coup against the Third World, starting with Chile in the early 1970s as their laboratory. For more, see Tricontinental: Institute for Social Research, The Coup Against the Third World: Chile, 1973, dossier no. 68, 5 September 2023, https://thetricontinental.org/dossier-68-the-coup-against-the-third-world-chile-1973/.
16 For more on SAPs and the role of debt in Africa, see Tricontinental: Institute for Social Research, Life or Debt: The Stranglehold of Neocolonialism and Africa’s Search for Alternatives, dossier no. 63, 11 April 2023, https://thetricontinental.org/dossier-63-african-debt-crisis.
17 World Bank, World Bank Development Report 1989: Financial Systems and Development (Washington, DC: World Bank, 1989); Era Dabla-Norris, ‘Financial Sector Deepening and Transformation’, in Frontier and Developing Asia (Washington, DC: International Monetary Fund, 2015), https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475595512/ch006.xml.
18 Samir Amin, The Implosion of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2014) and Tricontinental: Institute for Social Research, Globalisation and Its Alternative: An Interview with Samir Amin, notebook no. 1, 29 October 2019, https://thetricontinental.org/globalisation-and-its-alternative/.
19 Tricontinental: Institute for Social Research, The World in Economic Depression: A Marxist Analysis of Crisis, notebook no. 4, 10 October 2023, https://thetricontinental.org/dossier-notebook-4-economic-crisis/.
20 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government (New York: United Nations, 20 June 2024), https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024.
21 United Nations Conference on Trade and Development, Foreign Direct Investment and Development (New York: United Nations, 1999), https://unctad.org/system/files/official-document/psiteiitd10v1.en.pdf.
22 United Nations Conference on Trade and Development, Global Economic Fracturing and Shifting Investment Patterns (Washington, DC: United Nations, 23 April 2024), https://unctad.org/publication/global-economic-fracturing-and-shifting-investment-patterns.
23 Tricontinental: Institute for Social Research, Life or Debt.
24 Raghuram Rajan, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy (New Jersey: Princeton University Press, 2010), 93. For more on IMF policies and the Global South, see Tricontinental: Institute for Social Research, Life or Debt.
25 Raúl Prebisch, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems (New York: United Nations Economic Commission for Latin America, 1950). For more on Latin American structuralism, see Alfred Saad Filho, ‘The Rise and Decline of Latin American Structuralism and Dependency Theory’, in The Origins of Development Economics: How Schools of Economic Thought Have Addressed Development, edited by K. S. Jomo and E. S. Reinert (London: Zed Books, 2005).
26 Andre Gunder Frank, ‘The Development of Underdevelopment’, Monthly Review 18, no. 4, 1966.
27 Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (London: Verso, 1972).
28 Andre Gunder Frank, Crises in the Third World (New York: Holmes & Meier, 1967), 25.
29 Samir Amin, ‘A Note on the Concept of Delinking’, Review 10, no. 3 (Winter 1987): 435–444.
30 Benjamin Selwyn, ‘Why Global Value Chains Should Be Called Global Poverty Chains’, Developing Economics (blog), 13 January 2023, https://developingeconomics.org/2023/01/13/why-global-value-chains-should-be-called-global-poverty-chains/.
31 There are several exceptions to what we have said here, such as the work of Samir Amin on ‘delinking’ and the work of dependency theorists who operated in the early years of the Economic Commission of Asia (such as Ashok Mitra), the Economic Commission of Latin America (such as Osvaldo Sunkel, Theotônio dos Santos, and Vânia Bambirra), and the Economic Commission of Africa (such as Mekki Abbas and Robert K. A. Gardiner). See Tricontinental: Institute for Social Research, Dependency and Super-exploitation: The Relationship between Foreign Capital and Social Struggles in Latin America, dossier no. 67, 8 August 2023, https://thetricontinental.org/dossier-67-marxist-dependency-theory/.
32 Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975 (Stanford: Stanford University Press, 1982) and Alice H. Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialisation (Oxford: Oxford University Press, 1989).
33 The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy was published by the World Bank in 1993. It was authored by Nancy Birdsall, José Edgardo L. Campos, Chang-Shik Kim, W. Max Corden, Lawrence MacDonald, Howard Pack, John Page, Richard Sabor, and Joseph E. Stiglitz.
34 Ha-Joon Chang, The Political Economy of Industrial Policy (New York: St. Martin’s Press, 1994) and Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (London: Anthem Press, 2013).
35 The key text here is Nancy Birdsall and Frederick Jaspersen, eds., Pathways to Growth: Comparing East Asia and Latin America (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 1997).
36 Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: Verso, 1980).
37 Aijaz Ahmad, ‘Imperialism and Progress’, in Lineages of the Present: Political Essays (New Delhi: Tulika, 1996).
38 Robert Brenner, ‘The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism’, New Left Review, no. I/104 (July/August 1977): 25–92. Brenner’s essay occasioned a large debate, which began with Ben Fine’s ‘On the Origins of Capitalist Development’, New Left Review, no. I/109 (May/June 1978): 88–95 and Paul Sweezy’s short note ‘Comment on Brenner’, New Left Review, no. I/108 (March/April 1978): 94–95.
39 S. B. D. de Silva, The Political Economy of Underdevelopment (London: Routledge, 1982).
40 Sergei Tyulpanov, Politische Ökonomie und ihre Anwendung in den Entwicklungsländern [Political Economy and Its Application in the Developing States] (Frankfurt/Main: Verlag Marxistische Blätter, 1972).
41 Tricontinental: Institute for Social Research, Serve the People: The Eradication of Extreme Poverty in China, Studies in Socialist Construction no. 1, 23 July 2021, https://thetricontinental.org/studies-1-socialist-construction/.
42 Samir Amin, ‘China 2013’, Monthly Review 63, no. 10 (March 2013), https://monthlyreview.org/2013/03/01/china-2013/.
43 Enfu Cheng and Chan Zhai, ‘China as a “Quasi-Centre”’ in the World Economic System: Developing a New “Centre-Quasi-Centre-Semi-Periphery-Periphery” Theory’, World Review of Political Economy 12, no. 1 (Spring 2021): 22.
44 John Ross, Roy Singham, and Gisela Cernadas, “从210个经济体大数据中,我们发现了误解促消费对经济的危害” [From the Big Data of 210 Economies, We Found the Misunderstanding of Promoting Consumption to the Economy], Guancha, 21 October 2024, https://www.guancha.cn/LuoSiYi/2024_10_21_752447.shtml.
45 Vladimir Lenin, Lenin’s Collected Works, vol. 31 (Moscow: Progress Publishers, 1965), 408–426.
46 Amílcar Cabral, ‘The Weapon of Theory’, United Nations Economic Commission for Africa, African Institute for Economic Development and Planning, working paper, April 1978, https://repository.uneca.org/handle/10855/42836.
